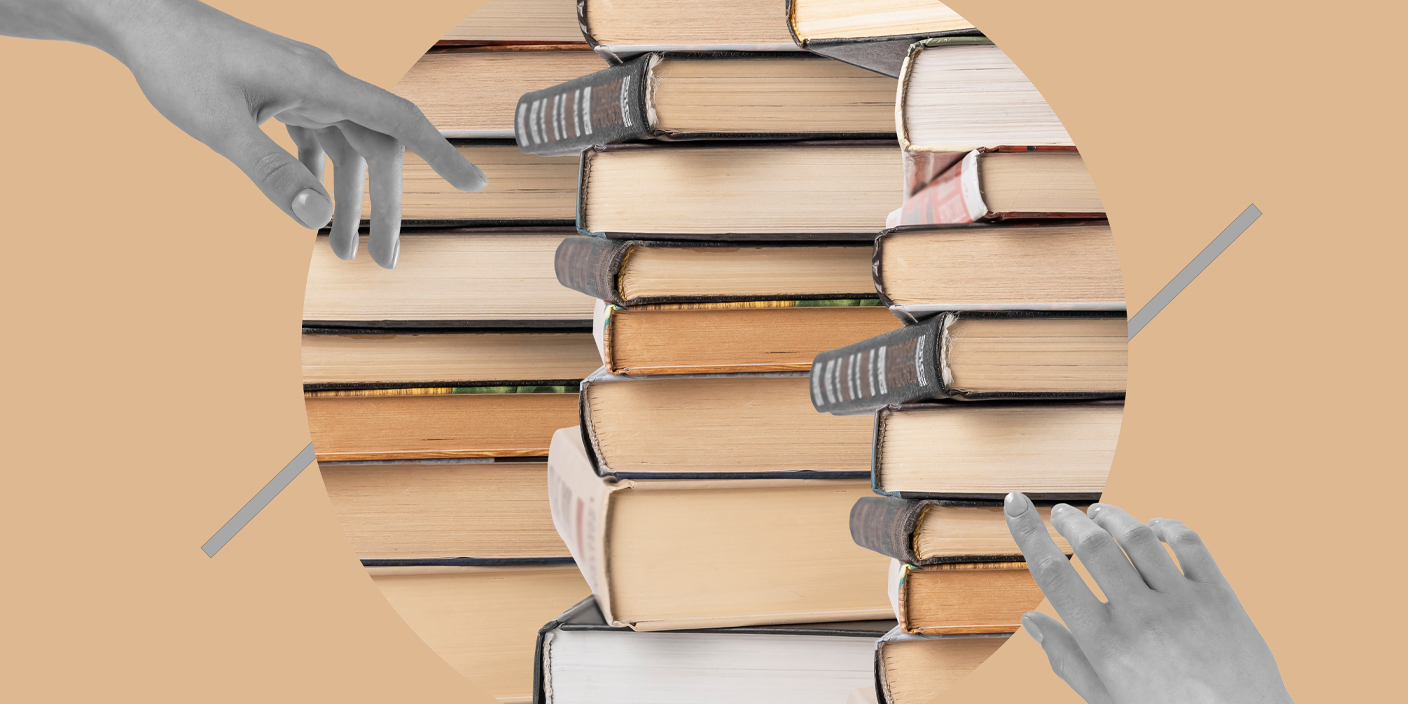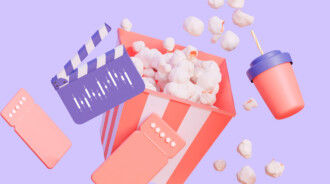क्योटो प्रोटोकॉल सामने आने वाली जलवायु परिवर्तन की स्थिति में हरित भविष्य की दिशा में मानवता के पहले महत्वपूर्ण कदम का प्रमाण है। आइए इस अभूतपूर्व समझौते की शुरुआत, उपलब्धियों और विरासत की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।
क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर युनाइटिड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौतों को बांधता है; प्रोटोकॉल का उद्देश्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों को सीमित करना है।
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। जापान के क्योटो में UNFCCC में पार्टियों के तीसरे सम्मेलन (COP3) में इस पर बातचीत की गई। यह सम्मेलन विकासशील देशों को स्वेच्छा से उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करता है जबकि अमीर देशों को उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों का पालन करने के लिए बाध्य करता है।
UNFCCC की स्थापना 1992 के रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। UNFCCC का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना था जो जलवायु प्रणाली को खतरनाक मानव प्रभाव से बचा सके। पहली COP 1995 में, बर्लिन में आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अमीर देशों को उत्सर्जन में कटौती करने की पहल करनी चाहिए। परिणामस्वरूप, 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल पर बातचीत की गई और इसे मंजूरी दे दी गई।
क्योटो प्रोटोकॉल को समझना
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) से संबंधित है। इसमें औद्योगिक देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया गया है।
इसके अनुसार, विकसित, औद्योगिकीकृत राष्ट्र 2012 तक अपने वार्षिक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में औसतन 5.2% की कटौती करने पर सहमत हुए। यह आंकड़ा दुनिया भर की सारी ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन के लगभग 29% के बराबर होगा।
जिन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया, उन्हें विशेष अवधि के लिए कार्बन उत्सर्जन सीमा दी गई और कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति दी गई। जिन देशों ने अपनी सीमा पार कर ली, उन्हें दंडित किया गया और अगली अवधि में उनकी आवंटित उत्सर्जन सीमा कम कर दी गई।
2012 तक, यूरोपीय संघ के सदस्य उत्सर्जन में 8% की कटौती करने पर सहमत हुए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा उत्सर्जन में क्रमशः 7% और 6% की कटौती करने पर सहमत हुए।
विकसित और विकासशील देशों के कर्तव्य
क्योटो प्रोटोकॉल ने माना कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का वर्तमान उच्च स्तर, जो 150 से अधिक वर्षों की आर्थिक गतिविधियों की वजह से है, के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक देश ज़िम्मेदार हैं। परिणामस्वरूप, विकसित देश कम विकसित देशों की तुलना में समझौते के तहत अधिक बोझ के अधीन थे।
यूरोपीय संघ सहित सैंतीस विकसित देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपने GHG उत्सर्जन को कम करना आवश्यक था। चीन और भारत सहित 100 से अधिक विकासशील देशों को क्योटो समझौते से पूरी तरह छूट दी गई और उन्हें स्वेच्छा से इसका अनुपालन करने के लिए आमंत्रित किया गया।
अनुलग्नक I बनाम गैर-अनुलग्नक I
क्योटो प्रोटोकॉल ने राष्ट्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया। अनुलग्नक I में धनी देश शामिल थे, और गैर अनुलग्नक I में विकासशील देश। समझौते के तहत केवल अनुलग्नक I के देश ही उत्सर्जन प्रतिबंधों के अधीन थे। भाग लेने वाली गैर-अनुलग्नक सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर उत्सर्जन को कम करने की पहल में भागेदारी की।
इन पहलों के माध्यम से, विकासशील देशों ने अपने समग्र कार्बन उत्सर्जन पर उच्च सीमा के बदले अमीर देशों को व्यापार करने या बेचने के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया। हालाँकि, इस समारोह ने औद्योगिक देशों को बड़ी मात्रा में GHG का उत्पादन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
क्योटो प्रोटोकॉल में अतिरिक्त बदलाव
क्योटो प्रोटोकॉल अंतिम नहीं था। बाद में दोहा संशोधन और पेरिस समझौता हुआ।
दोहा संशोधन: क्योटो प्रोटोकॉल 2020 तक बढ़ाया गया
प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि समाप्त होने के बाद मूल क्योटो समझौते के पूरक को स्वीकार करने के लिए दिसंबर 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल पार्टियाँ दोहा, कतर में एकत्रित हुईं। नए उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य पेश किए गए। हालाँकि, यह संशोधन केवल कुछ वर्षों तक ही चला।
2015 में, पेरिस सतत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान सभी UNFCCC पार्टियों ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया।
पेरिस का जलवायु समझौता
लगभग सभी देशों ने 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। सभी महत्वपूर्ण GHG-उत्सर्जक राष्ट्र अपने जलवायु-परिवर्तनकारी प्रदूषण को कम करने और समझौते के हिस्से के रूप में समय के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने पर सहमत हुए।

क्योटो प्रोटोकॉल आज
संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते के प्रमुख समर्थकों में से एक था। 2016 में इसे लागू किया गया और राष्ट्रपति ओबामा ने इसे “अमेरिकी नेतृत्व को श्रद्धांजलि” के रूप में सराहा।
डोनाल्ड ट्रम्प, जो उस समय राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे थे, ने इस समझौते को अमेरिकी लोगों के लिए एक भयानक सौदा बताया और निर्वाचित होने पर देश को हटाने का वादा किया। राष्ट्रपति बनने के बाद, ट्रम्प ने 2017 में घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ देगा क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
4 नवंबर, 2019 को पूर्व राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से समझौते से हटने की प्रक्रिया शुरू की। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की हार के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर, 2020 को पेरिस जलवायु समझौते से हट गया।
राष्ट्रपति बिडेन ने 20 जनवरी, 2021 को पदभार ग्रहण करते ही पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होना शुरू किया। यह समझौता 19 फरवरी, 2021 को प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल अब प्रभावी नहीं है, लेकिन इसके दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अभी भी कई कार्य किए जा रहे हैं।
समयरेखा
11 दिसंबर 1997 को अपनाए जाने के बाद 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तारीखें दी गई हैं।
11 दिसंबर, 1997
क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में COP3 में अपनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है। इसमें 159 देशों के प्रतिनिधि थे। क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती उद्देश्यों की स्थापना की गई है।
16 मार्च, 1998
क्योटो प्रोटोकॉल को 16 मार्च 1998 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हस्ताक्षर के लिए पेश किया गया था। राष्ट्रों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसके नियमों से बंधे रहने का अपना इरादा घोषित किया।
14 नवम्बर, 1998
ब्यूनस आयर्स कार्य योजना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए दो साल की योजना, दो सप्ताह के शिखर सम्मेलन के बाद 170 सरकारों द्वारा अपनाई गई है।
15 मार्च, 1999
एक वर्ष तक हस्ताक्षर के लिए खुले रहने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल पर 84 हस्ताक्षर हुए थे।
16 फरवरी, 2005
प्रोटोकॉल के वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुलग्नक I में सूचीबद्ध पर्याप्त देशों, कम से कम 55% औद्योगिक देशों, के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ।
दिसंबर 2005
कनाडा के मॉन्ट्रियल ने क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टियों की पहली बैठक (MOP 1) की मेज़बानी की। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में विकासशील देशों की सहायता के लिए पार्टियों द्वारा अनुकूलन कोष बनाया गया, और पार्टियों ने प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भी बहस की।
दिसंबर 2007
बाली एक्शन प्लान को इंडोनेशिया के बाली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अपनाया गया था। कार्य योजना ने 2012 के बाद की जलवायु व्यवस्था पर चर्चा का मार्ग प्रशस्त किया जो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगी।
8 दिसंबर, 2012
दोहा, कतर में पार्टियों के आठवें सम्मेलन (COP 18) सत्र में दोहा संशोधन को अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि (2013-2020) का गठन किया गया था, और उस समय सीमा के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य स्थापित किए गए थे।
25 मार्च, 2013
अफगानिस्तान ने 192वें राष्ट्र के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगस्त 2022 में, 192 हस्ताक्षरकर्ता मौजूद थे।
12 दिसंबर, 2015
क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाले पेरिस समझौते को पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के COP 21 सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी।
4 नवंबर, 2016
समझौता लागू किया गया। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश के इरादे से।
31 दिसंबर, 2020
147 देशों द्वारा नए प्रोटोकॉल को स्वीकार करने के बाद दोहा संशोधन लागू हुआ। ऐसा कहा गया था कि यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कम से कम 55% प्रतिनिधित्व करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नीचे दी गई है।
क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस समझौते में विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया गया।
किस देश ने अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन नहीं किया है?
एकमात्र राष्ट्र जिसने अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन नहीं किया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका ने 1998 में, समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अनुसमर्थन प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई। अमेरिकी सरकार ने 2001 में, यह चिंता जताते हुए कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित कर सकता है और चीन और भारत जैसे बड़े उभरते देशों ने उत्सर्जन में कटौती की प्रतिबद्धता नहीं जताई है, निर्णय लिया कि वह इस प्रोटोकॉल का अनुमोदन नहीं करेंगे।
क्योटो प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए?
क्योटो प्रोटोकॉल पर कुल 192 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संधि पर हस्ताक्षर करके, पार्टियों ने इसकी शर्तों का पालन करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। 16 मार्च, 1998 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालाँकि 192 देशों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उनमें से सभी ने इसकी पुष्टि नहीं की और संधि में शामिल नहीं हुए।
भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया?
क्योटो प्रोटोकॉल इन हिंदी पर 26 अगस्त, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 27 जनवरी, 2002 को प्रोटोकॉल की पुष्टि की। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और देश की आर्थिक वृद्धि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार करने के बाद सम्मेलन की पुष्टि की। एक विकासशील राष्ट्र के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत की प्रतिबद्धताएं उसके विकास उद्देश्यों के अनुरूप सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर केंद्रित थीं।
क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था?
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था। इसने क्योटो प्रोटोकॉल UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) परीक्षाओं को रुचि का एक महत्वपूर्ण बिंदु बना दिया। इसे निम्नलिखित कारणों से विकसित किया गया था:
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन;
- बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताएं;
- समान लेकिन विविध जिम्मेदारियाँ;
- सतत प्रथाओं का विकास;
- वैज्ञानिक सलाह;
- राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
निष्कर्ष
राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आवश्यक था। समझौते ने उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धताओं को स्थापित किया और जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक समझ को बढ़ाया।
हालाँकि, इसमें असफलताएँ भी थीं। राष्ट्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत थी। वे अपनी अर्थव्यवस्था से समझौता करने के अनिच्छुक थे। इसके कारण अपर्याप्त कार्बन कटौती हुई और वैश्विक गतिशीलता में बदलाव आया। इस प्रक्रिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
विश्व नेताओं ने क्योटो प्रोटोकॉल से सीखा है, और आने वाले समझौते ज़्यादा कुशल होंगे।